साहित्य कभी सियासत के सिरहाने, कभी पायताने
पता नहीं क्यों कवि-लेखक लोग कभी-कभी पुरस्कार लौटा देते हैं, यह जानते हुए भी कि अब तो साहित्यिक सम्मान भी प्रकारांतर से राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम हो चुके हैं। सत्ताएं सिर्फ दमन और शक्ति का ही प्रयोग नहीं करतीं, वे बौद्धिक चालाकी और काइआंपन को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका खेल चलता रहे। साहित्य में जन सरोकारों का होना कितना आवश्यक है, इससे किसी राजनेता को क्या लेना-देना।
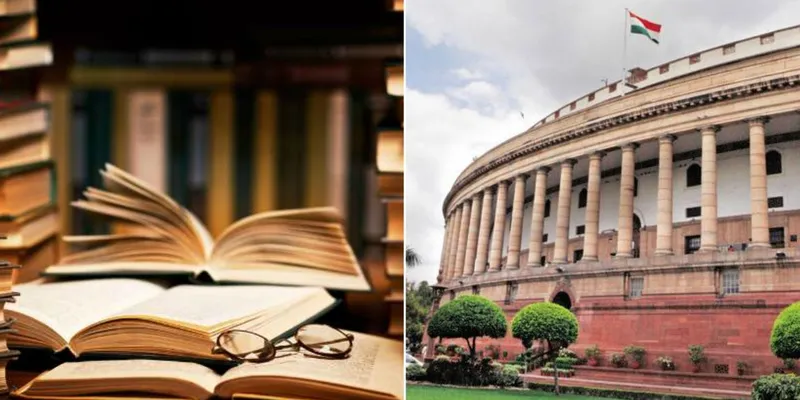
सांकेतिक तस्वीर
प्रेमचंद जेल तो नहीं गए लेकिन सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा अलबत्ता दे दिया। अगर इतिहास देखें तो साहित्य और राजनीति की यह पारस्परिकता नई नहीं है। संस्कृत साहित्य से परिचित लोग जानते हैं कि वाणभट्ट की कादंबरी में शुकनासोपदेश राजनीति के बारे में एक गंभीर उपदेश है।
कभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि साहित्य राजनीति का अनुचर नहीं, स्वतंत्र है। उसे पूरा अधिकार है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में से वह अपने कार्य के योग्य वे सभी द्रव्य उठा ले, जिन्हें राजनीति अपने काम में लाती है। अगर राजनीति अपनी शक्ति से सत्य की प्रतिमा गढ़कर तैयार कर सकती है तो साहित्य में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह उसके मुख में जीभ भर दे। पुरस्कारों की बात पर एक बाबूजी कहा करते थे कि भला घर आई हुई लक्ष्मी को भी कोई लौटाता है। दरअसल, आज का साहित्य बाजारवाद और राजनीति की गिरफ्त में है, लेकिन युवा रचनाकार आधुनिक उत्तर आधुनिक के इस दौर में भी समय और समाज का साक्षात्कार कर मानवीय अस्मिता और स्वतंत्रता को वाणी दे रहे हैं।
युवा पीढ़ी अपनी रचनाओं में समय का साक्षात्कार करती है और आधुनिक उत्तर आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को उजागर करती है। साहित्य और राजनीति की परस्परता सर्वस्वीकृत है। साहित्य में राजनीति अभिव्यक्ति पाती है, लेकिन साहित्य के लिए राजनीति हानिकारक है। युवा पीढ़ी मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति सजग और संघर्षशील है, उसे अनुकरण के बदले, साहनूभुति पर बल देना चाहिए और उसे ही अभिव्यक्त करना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने कभी लिखा था कि एक लेखक ने दादरी घटना के बाद साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाया, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि इसका दादरी घटना से क्या सम्बन्ध है।
धीरे-धीरे कुछ और साहित्यकारों ने भी लौटाया। ये खुद लौटा रहे हैं या एक-दूसरे को तैयार करते हैं ताकि सरकार के खिलाफ एक माहौल बने, क्योंकि दादरी में तो दो मरे, जिसकी जांच चल रही है, पर इससे पहले 1984 के दंगों में, भागलपुर के दंगों में, भोपाल गैस काण्ड में, मुजफ्फरनगर (यूपी) के दंगों में आपातकाल लगने पर, मुरादाबाद के दंगों में ये लोग चुप बैठे थे और अब सरकार बदलने पर ही यकायक इनकी आत्मा जाग गई, यह देखकर मुझे आश्चर्य और दुःख दोनों है। एक साहित्यकार ही ने मुझसे कहा कि ये लोग एक सरकार के शासन में अवार्ड ले लेते हैं और फिर उसी की वफादारी निभाने के लिए दूसरी सरकार जब आती है, तब ये उन्ही अवार्डों को वापस करने का दिखावा करते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत दुःख हुआ। किसी भी लिहाज़ से साहित्य अकादमी का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
साहित्य और राजनीति की इस मुठभेड़ से जरा आंखें फेरकर आइए, अब गोपाल प्रधान की बातों पर जरा गौर करते हैं। वह कहते हैं कि साहित्य की अतिरिक्त स्वायत्तता के पैरोकार और कविता की पवित्रता के आग्रही आम तौर पर साहित्य और राजनीति को आपस में दुश्मन साबित करके साहित्य को राजनीति से दूर रखने में ही उसकी भलाई समझते-समझाते हैं। सबसे अधिक उनका गुस्सा प्रगतिशील लेखकों पर उतरता है, जिन्होंने साहित्य और राजनीति के बीच उनके मुताबिक घालमेल किया और कविता जैसी नाजुक विधा को भी राजनीतिक बना डाला।
प्रगतिशील लेखन के इस अपराध का विरोध करने के लिए वे आश्चर्यजनक रूप से प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन में दिए गए प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण के एक अंश का ही सहारा लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। यह कथन प्रगतिवाद विरोधियों के लिए दोनों के बीच विरोध पैदा करने का अस्त्र और साहित्यकार के राजनीति से परहेज बरतने का बहाना बन जाता है। वे इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि खुद प्रेमचंद अपनी किताबों को स्वतंत्रता आंदोलन का अंग मानते थे। और शिवरानी देवी की मानें तो प्रेमचंद और उनके बीच होड़ लगी रहती थी कि कौन पहले जेल जाएगा।
प्रेमचंद जेल तो नहीं गए लेकिन सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा अलबत्ता दे दिया। अगर इतिहास देखें तो साहित्य और राजनीति की यह पारस्परिकता नई नहीं है। संस्कृत साहित्य से परिचित लोग जानते हैं कि वाणभट्ट की कादंबरी में शुकनासोपदेश राजनीति के बारे में एक गंभीर उपदेश है। प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र की रचना ही राजकुमारों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में राजनीति पर टिप्पणी की है। शूद्रक के मृच्छकटिकम (मिट्टी की गाड़ी)और विशाख के मुद्राराक्षस की बात ही क्या, ये तो शुद्ध रूप से राजनीतिक नाटक थे। आखिर क्यों साहित्य से राजनीति के जुड़ाव की यह दीर्घ परंपरा है?
साहित्य समूचे समाज से जुड़ा हुआ है जिसका एक अनिवार्य अंग राजनीति है इसलिए राजनीति से उसकी दूरी अस्वाभाविक है। तुलसीदास के रामराज्य की यूटोपिया को भी हम एक आदर्श राज्य का सपना मान सकते हैं उनके आदर्श की आलोचना के बावजूद। इस सुदीर्घ परंपरा ने ही वह जगह दी, जहाँ से प्रगतिशील लेखकों ने राजनीतिक साहित्य लिखना शुरू किया था। सवाल है कि जब राजनीतिक साहित्य की यह विशाल परंपरा थी ही तो प्रगतिशील लेखकों पर यह तोहमत क्यों कि उन्होंने साहित्य को उसके मूल धर्म से विलग कर दिया?
जितेन्द्र यादव बताते हैं कि एक साहित्यिक चर्चा में एक पत्रकार ने कहा कि साहित्य और राजनीति को अलग–अलग होना चाहिए। साहित्यकार को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कमोबेश इशारा साहित्यकारों के पुरस्कार वापसी की तरफ था। पुरस्कार वापसी एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि किन लेखकों ने किन कारणों से पुरस्कार लौटाएं किन्तु साहित्य और राजनीति को अलग–थलग करके देखना यह साहित्य और राजनीति दोनों का अति सरलीकरण माना जा सकता है। आजादी के पूर्व गुलामी के विरुद्ध लड़ाई साहित्यकारों और राजनेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, न खीचों कमानों को न तीर निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
यह आवाज गोरी सत्ता के खिलाफ साहित्यकरों ने दी थी। कई लेखक बगावती तेवर लिए हुए सिर्फ अख़बार और पत्रिकाएँ ही नहीं निकालते थे बल्कि उस समय के भारतीय राजनेताओं से सलाह–मशविरा भी करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पत्रिका द्वारा आजादी का अलख जगाना, प्रेमचन्द के कहानी संग्रह सोजे वतन पर प्रतिबन्ध लगाना इत्यादि दर्शाता है कि साहित्यकार राजनीति के प्रति कितने संजीदा थे। रामनरेश त्रिपाठी से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी तक कई कवियों ने जेल यात्राएं भी की। इंदिरा गाँधी के आपातकाल के खिलाफ नागार्जुन जैसे कवियों ने खूब जमकर लिखा और जेल की हवा भी खाई। वहीं फणीश्वरनाथ रेणु सरीखे साहित्यकारों ने पुरस्कार तक लौटा दिया।
हिन्दी कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि लेखकों को विरोध प्रदर्शन के लिए अलग रास्ता अपनाना चाहिए तथा स्वायत्त साहित्यिक संस्था का राजनीतीकरण नहीं करना चाहिए। आपात काल के दौरान भी अकादमी ने कोई रुख नहीं अपनाया था। लेखकों का सम्मान लौटाना ठीक इसलिए हो सकता है कि अगर देश में सच में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों के मानवाधिकार खतरे में पड़ रहे हैं, तो उनका कदम ठीक जरूर कहा जायेगा और इसलिए यह तर्क कोई मायने नहीं रखता कि आपातकाल के दौरान किसने क्या किया था?
इसके विपरीत अगर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को मुद्दा बनाकर कुछ साहित्यकार एक चुनी हुई बहुमत वाली सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तो यह वाकई गलत बात है। साहित्य का आज क्या स्तर रह गया है, यह किसी से छिपा हुआ तथ्य नहीं है। चेतन भगत जैसे लोग, जो हिंदी को रोमन में लिखने का बेतुका तर्क प्रस्तुत करते हैं और अपने उपन्यासों में मस्तराम का सुधरा संस्करण पेश करके वाहवाही लूट ले जाते हैं तो इसमें मठाधीश साहित्यकारों की असफलता ही छिपी हुई है।
आज का युवा वर्ग अगर किताबों से दूर गया है तो इसका सीधा मतलब यही है कि उसे उसके हिसाब से कंटेंट नहीं मिल रहा है और साहित्यकार अपनी बनाई एक आभाषी दुनिया में रचना करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसे कुछ पुरस्कार यह शासकीय वाहवाही मिल जाए। ऐसे में, बेवजह की राजनीति से साहित्य का और भी बेड़ागर्क होना तय है। कभी-कभी ऐसे वाकये हो जाया करते हैं, जब इस तरह के अभिमत और विमर्शों के लिए कोई जगह ही शेष नहीं दिखती है। मसलन, एक नामी साहित्यकार ने अपने से काफी कम उम्र के एक मुख्यमंत्री का पैर पकड़ लिया। बड़ा हो हल्ला मचा, खूब सारी बातें कही गयीं कि साहित्य तो राजनीति की दशा दिशा तय करता था, और अब वह राजनीति के चरणों में पड़ा हुआ है।
यूं भी साहित्यकारों की बदहाल आर्थिक स्थिति के बारे में किस्से बड़े पुराने हैं और उनके बारे में कहा यही जाता है कि जैसे चिराग खुद को जला कर रौशनी देता है, वैसे ही साहित्यकार खुद को जलाकर समाज की पीड़ा महसूस करते हैं और उससे दूसरों को रूबरू कराते हैं। ठीक ही तो है, सत्ता की दलाली करके तमाम ऐश-ओ-आराम का भोग करने वाले भला समाज का दर्पण कैसे बने रह सकते हैं! उनके चेहरे में तो अपने मालिक की तस्वीर ही दिखती है।
यह भी पढ़ें: जिस पद्मश्री गायिका के जागर गीतों का कभी लोगों ने किया था विरोध, उन्हें राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित







