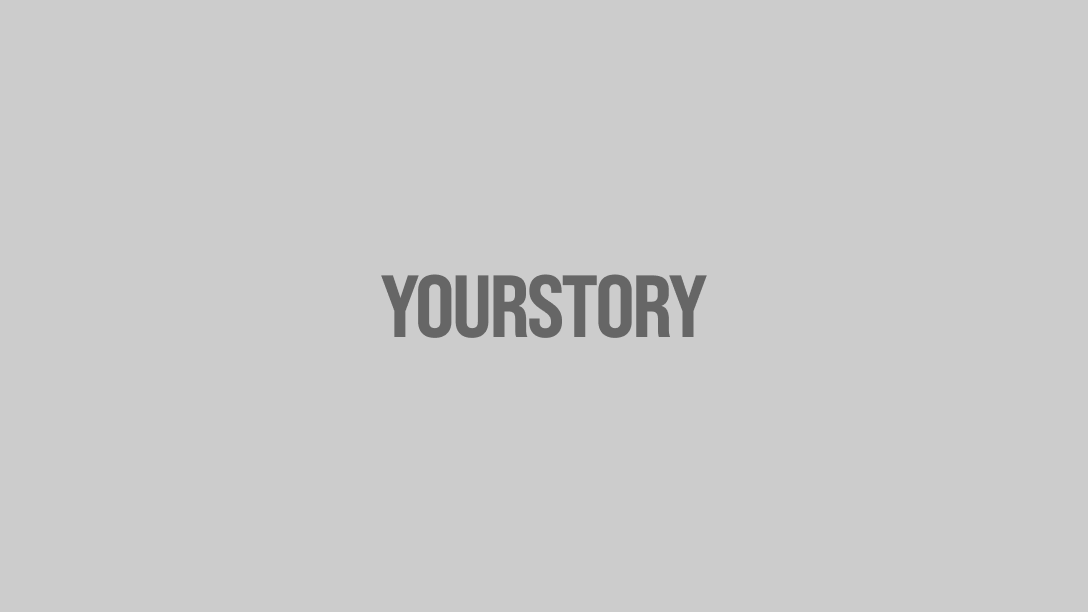कविता में नए-नए सौंदर्य तलाश रही हैं स्त्रियां
हिंदी कविता में भाषा का सबसे नया और सर्जनात्मक उपयोग कर रही हैं स्त्रियाँ: आशीष मिश्र
कविता में स्त्री की उपस्थितियों को रेखांकित करते हुए युवा आलोचक आशीष मिश्र कहते हैं कि आज हिंदी कविता में भाषा का सबसे नया और सर्जनात्मक उपयोग स्त्रियाँ ही कर रही हैं। वे पारंपरिक भाषा को बिना तोड़े अपने अनुभवों की कोडिंग ही नहीं कर सकतीं। अपने को रचने के लिए उन्हें एक नई भाषा और नये सौंदर्यशास्त्र की तलाश है।

सांकेतिक तस्वीर
शब्द और अवधारणाएँ दो ध्रुवीय हो सकती हैं, जीवन नहीं। इस तरह का विभाजन एक अवधारणात्मक सुविधा मात्र है परन्तु यह जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थापित समझ है।
साहित्य में स्त्री-विमर्श के तो कई सिरे हैं, हंस के संपादक एवं कथाकार राजेंद्र यादव के जमाने से इस पर पुरजोर बहसें भी चलती आ रही हैं लेकिन इधर सोशल मीडिया में कुछ और ही तरह की पिपहरी बज रही है। बजनी भी चाहिए, जब कविता में श्लीलता-अश्लीलता का प्रश्न सिर चढ़कर बोल रहा हो। ऐसी ही बहसों के बीच युवा आलोचक आशीष मिश्र सवाल उठाते हैं कि 'सर्जरी करवाने वाली स्त्रियां जीवन भर दवाएँ खाती हैं और बहुतेरे मामलों में कैंसर का शिकार होती हैं! फिर भी करवा रही हैं! वह कौन-सा दर्पण है, जहाँ वे खुद को देखती हैं, जो सिर्फ़ प्रतिछवि ही नहीं उपस्थित करता बल्कि उन्हें संपादित भी करता है। ये सौंदर्य- प्रतिमान कैसे बने? चिह्नों, संकेतों, प्रतीकों और छवियों का यह अदृश्य दर्पण कैसे बना? यह अदृश्य दर्पण लैंगिकता की द्वित्यात्मक विपर्ययी छवि द्वारा रचा जाता है। इस तरह के हिंसक ध्रुवीकरण में कलाओं की क्या भूमिका है? हिन्दी कविता ने इसमें कितना योग दिया है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है?'
आलोचक सुशील कुमार कहते हैं कि 'कवयित्री अनामिका ने अरसे से गांव को देखा नहीं। शुद्ध शहराती अनुभवों से पगी उनकी कविता स्त्री के अंग में कैंसर हो जाने की व्यथा से सम्बंधित है। इस कविता पर विद्वानों ने बहुत चर्चा की और कवयित्री को माथे पर चढ़ाया है पर क्या है इस कविता में? दरअसल, जब कवि के पास जीवन अनुभव नहीं होते तो वह नकली सम्वेदना के बल पर कविताएँ रचता है।' गौरतलब है कि स्त्री-प्रश्न पर ही इस साल साहित्य का नोबेल रद्द करने वाली विश्व प्रसिद्ध अकादमी का अपना भविष्य ही दांव पर लग गया है। अकादमी इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं देने की घोषणा कर चुकी है। स्वीडन की इस सम्मानित साहित्य अकादमी को ऐसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचाया है यौन दुराचार और भ्रष्टाचार ने। जर्मनी के पेन क्लब ने सुझाव दिया है- अकादमी वर्तमान संकट का लाभ उठा कर अपना संपूर्ण कायाकल्प कर डाले और अंतरराष्ट्रीय सहित्यकारों को भी अपनी पांत में शामिल करे।
आज की हिंदी कविता में स्त्री की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए आशीष मिश्र का कहना है कि शब्द और अवधारणाएँ दो ध्रुवीय हो सकती हैं, जीवन नहीं। इस तरह का विभाजन एक अवधारणात्मक सुविधा मात्र है परन्तु यह जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थापित समझ है। इसके लिए तथ्य और तर्क की ज़रूरत नहीं है। ‘जेंडर बाइनरिज़्म’ दोनों ध्रुवों के बीच पड़ने वाली सारी चीज़ों को परिधि पर फेंक देता है। यह स्थापित करता है कि स्याह और सफ़ेद के बीच दूसरे रंग नहीं होते। यह यौनिकता को तमाम रंगों की एक पट्टी मानने के बजाय दो स्थायी रंगों में कील देता है। सौंदर्यबोध के स्तर पर यह समान्य व्यवहार का हिस्सा है और कवि समय की तरह प्रचलित है।
पूरा सौंदर्यशास्त्र इस दो-ध्रुवीय युग्म को मज़बूत करता है। निराला की कविता जूही की कली को ध्यान से पढ़ें। पवन और कली के बीच का पूरा संबंध इसी ‘जेंडर बाइनरिज्म’ से निर्मित है। कविता में जुही की कली एक निष्क्रिय देह में बदल जाती है। ‘निर्दय’ और ‘निपट निठुराइ’ शब्द बहुत सकारात्मक अर्थ देने लगते हैं! और पाठक इसका आनन्द लेता है। रामविलास शर्मा ने रागविराग में छठी कविता के रूप में जिस कविता को चुना है। कविता का विश्लेषण करना बिम्ब-प्रतीकों और लय पर बात करने के साथ सौंदर्य के इस राजनीति को उद्घाटित करना है।
स्त्री-कविता को विश्लेषित करना कठिन लेकिन ज़रूरी है। कठिन इसलिए कि स्त्री है तो अनुभूत के नाते प्रामाणिक मानने का सहज आग्रह भी है। दूसरे पुंसवाद स्त्रीवादी नारों के नीचे छिपा होता है। ज़रूरी इसलिए है कि इस तरह की आरोपित निर्मिति उनके स्व का ही निषेध करती है। यह देखना सुखद है कि आज स्त्रियाँ इन चीज़ों के प्रति धीरे-धीरे सजग हो रही हैं। वे भाषा में पुंसवादी सौंदर्यबोध को उलट रही हैं। वे दिन और सूर्य के सुंदरीकरण के बजाय रात और प्रकाश के विविध शेड्स को रचती हैं। वे हर जगह हर स्तर पर लैंगिक ध्रुवीकरण को तोड़ रही हैं। वे प्रकृति को नई भाषा की तरह रचती हैं। वे मिथकों को पुनर्व्यख्यायित कर रही हैं। वर्तमान में भाषा का सबसे नया और सर्जनात्मक उपयोग स्त्रियाँ ही कर रही हैं। वे पारंपरिक भाषा को बिना तोड़े अपने अनुभवों की कोडिंग ही नहीं कर सकतीं। अपने को रचने के लिए उन्हें एक नई भाषा और नये सौंदर्यशास्त्र की तलाश है।
ख्यात आलोचक सुशील कुमार कविता में स्त्री प्रश्न को एक नए सिरे से उठाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम लेखन में 'प्रोग्रेसिव' होने की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी लगता है कि प्रगतिशीलता का भारतीय चित्त पाश्चात्य संस्कार व संस्कृति से बिल्कुल विच्छिन्न है। यह विज्ञान नहीं कि उसके आगे काम करने के लिए उसकी 'थ्योरी' को सीखना जरूरी है लेकिन हमारे यहां जो आनंदवादी और कल्पनावादी कवियों की फौज है, जिसने प्रगतिशीलता को अपने आभिजात्य संस्कार का शिकार बनाया है, उसने प्रगतिशील विचारधारा को काटकर स्त्री-मुक्ति विषयक विचारों की अलग श्रेणी का निर्माण कर लिया और इसे 'स्त्री-विमर्श' की संज्ञा से नवाजा। उनका यह विमर्श पश्चिमी विचारबोध का पिछलग्गू है, उसकी उधार वृत्ति है और उसी को अपना आदर्श मानता है। शिवमूर्ति, अखिलेश, पवन करण, अनामिका आदि इसी श्रेणी के साहित्यकार हैं, जिनमें यौनिकता के प्रति जो आकर्षण है, उसके पीछे उनकी दमित वासना का विकृत मन है।
इसी मन से ये स्त्रीकामी कवि उसकी मुक्ति के सवाल को आगे रखकर प्रोग्रेसिव होने का ढोंग और ढंग रचते हैं और बड़ी बेहयाई से स्त्री-अंगों को अपनी कलम की वासना का शिकार बनाते हैं। स्त्री देह पर अश्लील कविताएं लिखने का भला क्या सामाजिक औचित्य है? इसमें किस जनचेतना का प्रतिफलन होता है? आज ब्रेस्ट कैंसर से अधिक प्रोस्टेट कैंसर होता है। उस पर कविताएँ क्यों नहीं लिखी जातीं? उत्तरआधुनिक सोच से उपजी ऐसी कविताओं में जरा भी भारतीय चित्त नहीं है। दूसरे, शिल्प की दृष्टि से लद्धड़ गद्यनुमा कविता तो है ही। अनामिका हिंदी की वरिष्ठ कवयित्री हैं।
उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद् पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारतभूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है लेकिन उनकी कविताओं में निराश मन का गहन अवसाद है। क्या कविता का काम सेक्स के माध्यम से जुगुप्सा उत्पन्न करते हुए दमित कुंठाओं को परोसना है? उनकी कविता किसी स्त्री की पीड़ा का प्रतिदर्श रचती है या फिर कवयित्री की व्यक्तिगत मनोदशा को उसकी कुंठा में तब्दील करती है? एक आदिवासी महिला बबीता टोप्पो को समर्पित उनकी एक कविता क्या बीमारी से लड़ने के उसके संघर्ष को व्यापकता से दिखाने में सक्षम हुई है? महिला होकर अनामिका ने एक पीड़ित नारी की व्यथा-जगत को सेक्स-रंजित कर कविता को रीतिकाल की ओर मोड़ने का काम किया है। मैं तो इसे कविता का सामंतीकरण मानता हूँ।
यह भी पढ़ें: कितनों को याद होगा विद्रोही अरुणा आसफ़ अली का नाम!